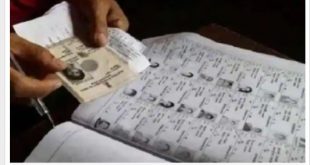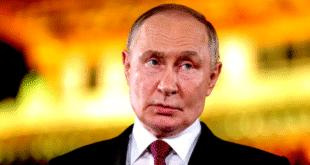अशोक कुमार
उच्च शिक्षा संस्थानों, विशेषकर विश्वविद्यालयों में, शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति में देरी एक गंभीर और बहुआयामी समस्या है। इसमें कई बार कुलपतियों (Vice-Chancellors – VCs) द्वारा जानबूझकर की जाने वाली देरी की भी भूमिका होती है। यह सिर्फ प्रशासनिक अक्षमता का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई जटिल कारण हो सकते हैं:

जानबूझकर देरी के संभावित कारण
कुलपतियों द्वारा पदोन्नति में जानबूझकर देरी करने के कुछ मुख्य कारण ये हो सकते हैं:
राजनीतिक हस्तक्षेप और पक्षपात:
चहेतों को लाभ: कुलपति कई बार अपने राजनीतिक आकाओं या व्यक्तिगत चहेतों को समायोजित करने के लिए नियुक्तियों या पदोन्नति को रोक सकते हैं, ताकि उनके पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए रास्ता बनाया जा सके।
सत्ता का दुरुपयोग: कुलपति अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके उन शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित कर सकते हैं जिनसे उनके व्यक्तिगत या राजनीतिक मतभेद हों। नियंत्रण बनाए रखना: कुछ कुलपति देरी करके या नियमों को तोड़-मरोड़ कर शिक्षकों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं।
आर्थिक और वित्तीय दबाव:
वित्तीय लाभ: कुछ मामलों में, देरी करके या पदोन्नति को रोककर वित्तीय लाभ कमाने की कोशिश की जा सकती है, जैसे किसी विशेष सलाहकार या बाहरी व्यक्ति को भुगतान करना।
बजट की कमी: विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त बजट न होने पर भी कुलपति पदोन्नति को टाल सकते हैं, ताकि वेतन वृद्धि के अतिरिक्त बोझ से बचा जा सके। यह जानबूझकर न होकर मजबूरी का नतीजा हो सकता है, लेकिन इसका परिणाम देरी ही होता है।
* प्रशासनिक जटिलताएं और अक्षमता (जो जानबूझकर भी हो सकती है):
अधिकारों का केंद्रीकरण: कई बार कुलपति सभी निर्णय अपने हाथ में रखना चाहते हैं, जिससे प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं।
जटिल प्रक्रियाएं: पदोन्नति की प्रक्रियाएं इतनी लंबी और जटिल होती हैं कि जानबूझकर देरी करने के लिए उनमें आसानी से loopholes (कमजोरियाँ) मिल जाती हैं।निर्णय लेने में अनिच्छा: विवादास्पद मामलों या कानूनी उलझनों से बचने के लिए भी कुछ कुलपति निर्णय लेने में देरी करते हैं।
कार्यकाल का प्रभाव:
कार्यकाल के अंत में: जब कुलपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है, तो वे बड़े निर्णय लेने से बच सकते हैं, या फिर केवल उन नियुक्तियों और पदोन्नति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो उनके लिए फायदेमंद हों।
देरी के व्यापक कारण (जानबूझकर के अलावा)
कुलपतियों की भूमिका के अलावा, शिक्षकों की पदोन्नति में देरी के कई अन्य संस्थागत और संरचनात्मक कारण भी हैं:
सरकारी और नियामक बाधाएं:
नोडल एजेंसियों का हस्तक्षेप: उच्च शिक्षा के लिए कई नोडल एजेंसियां (जैसे UGC, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारें) होती हैं, जिनके बीच समन्वय की कमी और overlapping (अतिव्यापी) जिम्मेदारियां देरी का कारण बनती हैं।
नियमों में अस्पष्टता: पदोन्नति के नियमों और दिशानिर्देशों में अस्पष्टता या बार-बार बदलाव से भी प्रक्रियाएं बाधित होती हैं।
खाली पद: केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हजारों और राज्य विश्वविद्यालयों में 40% से अधिक शिक्षण पद खाली हैं। खाली पदों को भरने की प्रक्रिया ही इतनी धीमी होती है कि पदोन्नति के अवसर भी कम हो जाते हैं।
कानूनी मुकदमेबाजी:
न्यायालयीन हस्तक्षेप: नियुक्तियों या पदोन्नति से संबंधित विवादों के कारण कई बार मामले न्यायालयों में चले जाते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया रुक जाती है। आरक्षण नीतियों, पात्रता मानदंडों या चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर अक्सर मुकदमे दायर होते हैं।
प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार:
लंबित फाइलें: विश्वविद्यालयों के अंदर फाइलों का लंबित रहना, नौकरशाही की सुस्ती, और नियुक्तियों एवं पदोन्नति समितियों की निष्क्रियता आम समस्याएं हैं।
पारदर्शिता की कमी: चयन और पदोन्नति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी भी देरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है।
संसाधनों की कमी:
वित्तीय बाधाएं: कई विश्वविद्यालयों को वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे वे नए पद सृजित करने या पदोन्नत शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन देने में असमर्थ होते हैं।
बुनियादी ढांचे का अभाव: अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और डिजिटल संसाधनों की कमी भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को धीमा करती है।
देरी का प्रभाव
शिक्षकों की पदोन्नति में देरी के गंभीर परिणाम होते हैं:
शिक्षा की गुणवत्ता पर असर: योग्य शिक्षकों की कमी और मौजूदा शिक्षकों पर काम का बोझ बढ़ने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
अनुसंधान में कमी: शिक्षकों को पदोन्नति के लिए प्रोत्साहन न मिलने से वे अनुसंधान और उच्च स्तरीय शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते।
नैतिक पतन: पदोन्नति में अनिश्चितता और देरी से शिक्षकों में निराशा, नैतिक पतन और प्रेरणा की कमी आती है।
विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली: फैकल्टी की कमी से कक्षाओं में भीड़भाड़, अकादमिक कैलेंडर में देरी और समग्र रूप से विश्वविद्यालय का कामकाज बाधित होता है।
प्रतिभा पलायन: योग्य शिक्षक बेहतर अवसरों की तलाश में अन्य संस्थानों या देशों का रुख कर सकते हैं।
समाधान के प्रयास और चुनौतियाँ
सरकार और UGC ने इस समस्या के समाधान के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जैसे:
UGC ड्राफ्ट रेगुलेशंस 2025: नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, लचीलापन लाने और चयन मानदंडों को अधिक समग्र बनाने का प्रस्ताव है। हालांकि, कुछ आलोचकों का मानना है कि ये नियम संविदाकरण (contractualization) को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा प्रभावित होगी।
पारदर्शिता बढ़ाना: कई जगहों पर ऑनलाइन आवेदन और चयन प्रक्रियाओं को अपनाने की बात हो रही है।
हालांकि, इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता में वृद्धि और पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। केवल तभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की समय पर नियुक्ति और पदोन्नति सुनिश्चित की जा सकेगी।
(लेखक पूर्व कुलपति कानपुर , गोरखपुर विश्वविद्यालय , विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर)
 Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal
Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal