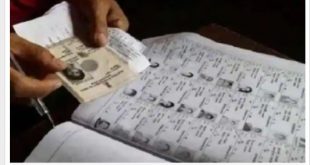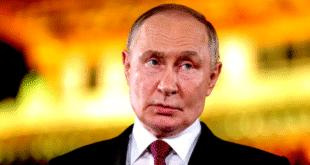अशोक कुमार
राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई नई नीति, जिसके अंतर्गत राज्य के 335 राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्यों की नियुक्ति पांच वर्षों के अनुबंध पर की जाएगी, न केवल शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाली नीति है, बल्कि यह उच्च शिक्षा की मूल आत्मा और UGC के मूल उद्देश्यों के भी प्रतिकूल है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देशभर में उच्च शिक्षकों के लिए जो वेतनमान निर्धारित किए हैं, वे सामान्य सेवाओं से कहीं अधिक हैं और इसके पीछे एक स्पष्ट सोच रही है — देश के श्रेष्ठतम मस्तिष्कों को शिक्षा और अनुसंधान की दिशा में प्रेरित करना। क्योंकि जब शिक्षक सामाजिक, आर्थिक और कार्यस्थल की दृष्टि से सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं, तभी वे शिक्षण, शोध और नवाचार में अपनी ऊर्जा और समर्पण दे सकते हैं।
राजस्थान की नई नीति में शिक्षकों को केवल 28,000 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त किया जाएगा, जो कि UGC द्वारा निर्धारित 57,700 रुपये न्यूनतम वेतन के लगभग आधे से भी कम है। यह स्थिति न केवल शिक्षकों की गरिमा के विरुद्ध है, बल्कि इससे युवाओं में उच्च शिक्षा को करियर विकल्प के रूप में चुनने की इच्छा भी क्षीण होगी। एक तरफ हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम शिक्षकों को अस्थायी संविदा पर अल्प वेतन में कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं, जो स्पष्ट रूप से दोहरी मानसिकता को दर्शाता है।
शिक्षा केवल नौकरी नहीं होती, वह समाज निर्माण का कार्य है। एक सहायक आचार्य जब कॉलेज में प्रवेश करता है, तो वह विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता, बल्कि उन्हें जीवन के उच्च मूल्यों, शोध की संस्कृति और नवाचार की दिशा में भी मार्गदर्शन देता है। यदि उसका स्वयं का भविष्य अनिश्चित हो, तो वह अपने छात्रों को स्थायित्व और लक्ष्य की प्रेरणा कैसे दे पाएगा?
विद्या संबल योजना को समाप्त करने और गुजरात मॉडल के आधार पर संविदा शिक्षक नियुक्त करने का निर्णय यह दर्शाता है कि सरकार तात्कालिक वित्तीय प्रबंधन को दीर्घकालिक शिक्षा नीति पर वरीयता दे रही है। क्या शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं जिनमें शिक्षकों की योग्यता, सुरक्षा और प्रेरणा के साथ समझौता हो?
राजकीय महाविद्यालय पहले ही शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। शोध, नवाचार और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार तभी संभव है जब योग्य शिक्षक स्थायित्व और सम्मान के साथ कार्य कर सकें। तीन वर्षों के अंतराल पर प्राचार्यों का कार्यकाल बढ़ाने की योजना भी केवल पद की निरंतरता को सुनिश्चित करती है, न कि संस्था की गुणवत्ता को।
आवश्यक है कि पदस्थापन और सेवा विस्तार की कोई भी योजना केवल अनुभव नहीं बल्कि निष्पक्ष मूल्यांकन के आधार पर हो।यह नीति केवल एक शॉर्टकट समाधान है, जो दीर्घकालिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और स्थायी बनाना होगा। शिक्षकों को राष्ट्रीय वेतनमान, सेवा सुरक्षा और शोध के लिए सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। तभी हम एक ऐसा शिक्षण तंत्र विकसित कर सकते हैं जो भारत को वैश्विक ज्ञान-शक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर हो सके।
शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए शिक्षक की भूमिका केंद्रीय है। यदि हम शिक्षा को भविष्य का निवेश मानते हैं, तो हमें शिक्षकों को केवल संविदा कर्मी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता के रूप में देखना होगा।
(लेखक पूर्व कुलपति कानपुर , गोरखपुर विश्वविद्यालय , विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर रह चुके हैं)
 Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal
Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal