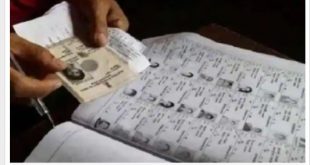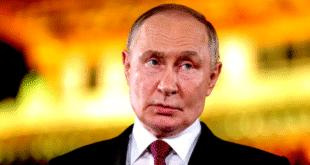अशोक कुमार
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में शिक्षा में नवाचार, विशेषकर डिजिटलीकरण और AI जैसी प्रौद्योगिकियों के एकीकरण पर बहुत जोर दिया गया है, और यह उम्मीद की गई थी कि इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षण संस्थानों को बेहतर आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी। हालांकि, जैसा कि आपने अनुभव किया है, जमीनी स्तर पर यह अपेक्षा पूरी तरह से पूरी होती नहीं दिख रही है।
NEP 2020 में शिक्षा में नवाचार के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण है, लेकिन इसे लागू करने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रतिबद्धता, विशेषकर राज्य सरकारों की ओर से, अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जब तक केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा को एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में नहीं देखतीं और इसके लिए पर्याप्त बजट आवंटित नहीं करतीं, तब तक NEP के नवाचार संबंधी लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त करना मुश्किल होगा।

राज्य सरकारें विश्वविद्यालयों को पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं दे रही हैं ! एक ओर सरकार कहती है कि विश्वविद्यालय अपनी आय के स्रोत बढ़ाएँ: इसका मतलब है कि विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम, परामर्श सेवाएं, अनुसंधान परियोजनाएं, या अन्य माध्यमों से धन जुटाएं। सरकार चाहती है कि विश्वविद्यालय अपनी वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ाएं और पूरी तरह से सरकारी अनुदान पर निर्भर न रहें।
विश्वविद्यालय एक तरफ तो आय बढ़ाने के लिए दबाव में हैं, और दूसरी तरफ, जब वे अपनी मेहनत से आय अर्जित करते हैं, कई राज्यों में सरकार इस आय का 25 प्रतिशत हिस्सा ले लेती है यह उनकी वित्तीय स्थिति को और कमजोर हैं ! उनके पास अपने विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने या छात्रों को सुविधाएं देने के लिए बहुत कम पैसा बचता है। इसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है।
अंततः, इस वित्तीय कमी का बोझ छात्रों पर ही पड़ता है। विश्वविद्यालय और कॉलेज अपनी आय की कमी को पूरा करने के लिए फीस बढ़ाते हैं, जिससे स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों की फीस और भी अधिक हो जाती है, जैसा कि हमने पहले चर्चा की। यह गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को और भी दुर्गम बना देता है।
सरकार का उद्देश्य विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाना हो सकता है, लेकिन इस तरह से आय का एक हिस्सा वापस लेना इस लक्ष्य को कमजोर करता है। यह विश्वविद्यालयों को अपनी पूरी क्षमता से काम करने से रोकता है। सरकार को विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें पर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता भी देनी चाहिए ताकि वे अपनी आय का उपयोग शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के कल्याण के लिए कर सकें। विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें बिना योजना के स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम चलाने पड़ रहे हैं।
इसका सीधा असर छात्रों पर पड़ता है, खासकर गरीब छात्रों पर, क्योंकि उन्हें इन पाठ्यक्रमों के लिए उच्च शुल्क देना पड़ता है।विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अपने खर्च चलाने के लिए छात्रों से ट्यूशन, परीक्षा और अन्य संबद्धता शुल्क के नाम पर ज़्यादा पैसे लेने पड़ते हैं।कॉलेजों को विश्वविद्यालयों से संबद्धता बनाए रखने के लिए भी ज़्यादा शुल्क देना पड़ता है, और वे इस लागत को भी छात्रों से वसूलते हैं।यह सब मिलकर गरीब और वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को मुश्किल बना देता है। शिक्षा एक अधिकार है, लेकिन इन शुल्कों के कारण यह एक महंगी वस्तु बन गई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का शोषण होता है।
यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का भी सवाल है। जब उच्च शिक्षा महंगी हो जाती है, तो यह समाज के एक बड़े वर्ग के लिए पहुंच से बाहर हो जाती है। इससे गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं, जिससे गरीबी और असमानता का दुष्चक्र चलता रहता है।
इस समस्या को हल करने के लिए कई स्तरों पर काम करना होगा: सरकारी फंडिंग में वृद्धि: सबसे ज़रूरी है कि राज्य सरकारें विश्वविद्यालयों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दें। शिक्षा को निवेश के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि सिर्फ खर्च के तौर पर। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अपने शुल्क ढांचे को पारदर्शी बनाना चाहिए और हर शुल्क के पीछे का कारण स्पष्ट करना चाहिए। नियामक निकायों को कॉलेजों द्वारा मनमाने ढंग से शुल्क वसूलने पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और उन्हें रोकना चाहिए।
आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता योजनाएं शुरू की जानी चाहिए।छात्र संघों, अभिभावक समूहों और नागरिक समाज संगठनों को मिलकर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि शिक्षा के लिए सार्वजनिक फंडिंग बढ़ाई जाए और स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों को विनियमित किया जाए। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ध्यान देने और ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि उच्च शिक्षा सभी के लिए सुलभ और सस्ती बन सके, न कि केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए।
राजस्थान के कई विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को पेंशन न मिलने या भविष्य में इसकी संभावना कम होने की समस्या गंभीर है, और इस पर राज्य सरकार की ‘शांति’ या निष्क्रियता कई सवाल खड़े करती है। यह सिर्फ कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा संस्थानों के भविष्य और उनमें काम करने वाले लोगों के मनोबल से भी जुड़ा है।
कई विश्वविद्यालय सीधे राज्य सरकार के तहत आते हैं। यदि सरकार विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को सीधे पेंशन देने की जिम्मेदारी नहीं लेती है या इसमें देरी करती है, तो यह विश्वविद्यालयों के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है, खासकर जब वे स्वयं भी वित्तीय संकट से जूझ रहे हों।
विश्वविद्यालयों की अपनी आय का उपयोग:
जैसा कि हमने पहले चर्चा की, यदि विश्वविद्यालय अपनी आय का एक हिस्सा , 25 % सरकार को देते हैं, तो उनके पास कर्मचारियों को पेंशन देने या उनके भविष्य निधि में योगदान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं बचता। राजस्थान के विश्वविद्यालय में लड़कियों और कुछ आरक्षित वर्ग के छात्रों से सामान्य छात्रों की तुलना में कम फीस ली जाती है, लेकिन सरकार द्वारा इस कम फीस का पूरी तरह से पुनर्भरण नहीं किया जाता, जबकि कई अन्य राज्यों में सभी छात्रों की फीस समान होती है और आरक्षित वर्ग के छात्रों को सीधे सरकार द्वारा पुनर्भरण मिल जाता है। यदि सरकार आय का 25 प्रतिशत न काटे और आरक्षित वर्ग की फीस का पुनर्भरण कर दे तब करामचरियों की पेंशन की समस्या का हल हो सकता है !पर्याप्त सरकारी सहायता के बिना डिजिटल नवाचारों में निवेश करते हैं, तो अंततः इसका बोझ छात्रों पर फीस वृद्धि के रूप में पड़ सकता है।
पेंशन न मिलना या अनिश्चितता कर्मचारियों के लिए कई तरह से हानिकारक है:सेवानिवृत्ति के बाद की आय की अनिश्चितता कर्मचारियों में भय और चिंता पैदा करती है, खासकर जब उन्हें अपनी बचत पर निर्भर रहना पड़े। जब कर्मचारी यह देखते हैं कि उनकी दशकों की सेवा के बाद उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही है, तो उनका मनोबल गिरता है, जिससे उनके काम की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।योग्य और अनुभवी शिक्षक तथा कर्मचारी ऐसे संस्थानों की तलाश कर सकते हैं जहाँ बेहतर सेवानिवृत्ति लाभ और वित्तीय सुरक्षा हो, जिससे राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रतिभा की कमी हो सकती है।
राज्य सरकार की ओर से इस मुद्दे पर ‘शांति’ या निष्क्रियता कई बातें दर्शाती है:हो सकता है कि सरकार के लिए कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा अन्य राजनीतिक या आर्थिक प्राथमिकताओं की तुलना में कम महत्वपूर्ण हो।सरकार स्वयं वित्तीय दबाव में हो सकती है और इस मुद्दे को हल करने के लिए तत्काल कोई समाधान न हो। सरकार इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट नीतिगत निर्णय नहीं ले पा रही हो, या वह विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही हो जिसमें समय लग रहा हो। कर्मचारियों के भविष्य से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे को हल करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी हो सकती है।
ये भी पढ़ें-महिला सशक्तिकरण के लिए रूढ़िवादी बंधनों से मुक्ति जरूरी
यह स्थिति उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक बड़े संकट की ओर इशारा करती है। सरकार को जल्द से जल्द इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के पेंशन के लिए एक स्थायी और सम्मानजनक समाधान खोजना चाहिए ताकि उनके भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
(लेखक पूर्व कुलपति कानपुर , गोरखपुर विश्वविद्यालय , विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर रह चुके हैं)
 Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal
Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal