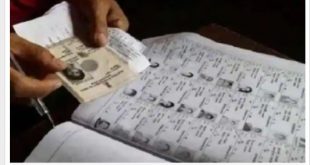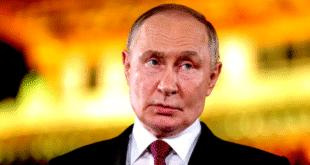अशोक कुमार
वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में स्कूलों को बंद करने और विलय करने की प्रक्रिया चल रही है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का रुझान बन गया है, जिसके पीछे कई कारण और तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएं भी हैं।

मुख्य कारण जो बताए जा रहे हैं:
कम छात्र संख्या : यह सबसे बड़ा कारण है। कई सरकारी स्कूल, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में, बहुत कम छात्रों के साथ चल रहे हैं। कुछ मामलों में तो शून्य छात्र संख्या वाले स्कूल भी पाए गए हैं (जैसा कि राजस्थान में देखा गया)। सरकार का तर्क है कि इन स्कूलों को बनाए रखना संसाधनों का अपव्यय है।
संसाधनों का बेहतर उपयोग: सरकार का मानना है कि छोटे-छोटे स्कूलों में बिखरे हुए शिक्षकों, कक्षाओं और अन्य बुनियादी ढांचे को एक जगह लाकर उनका बेहतर और अधिक कुशल उपयोग किया जा सकता है। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी।
प्रशासनिक खर्चों में कमी : कम स्कूलों का प्रबंधन करना, उनका निरीक्षण और ऑडिट करना सरकार और शिक्षा विभाग के लिए आसान होता है, जिससे प्रशासनिक लागत कम होती है।
शिक्षकों का बेहतर उपयोग : जहां शिक्षकों की कमी है, वहां विलय के बाद शिक्षकों को उन स्कूलों में स्थानांतरित किया जा सकता है जहां छात्रों की संख्या अधिक है, जिससे शिक्षक-छात्र अनुपात बेहतर हो सकता है।
गुणवत्ता में सुधार का तर्क : तर्क दिया जाता है कि बड़े स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढांचा, अधिक शिक्षण सामग्री , ई-लर्निंग सुविधाएं और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियां उपलब्ध होंगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
विभिन्न राज्यों में स्थिति और रुझान:
उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में हाल ही में स्कूलों को बंद करने या विलय करने का निर्णय लिया गया है। जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 50 से कम है, उन्हें विलय किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी स्कूल एकीकरण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि स्कूल एक किलोमीटर के भीतर ही स्थापित किया जाए।
राजस्थान: राजस्थान में भी शून्य छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद किया गया है और कुछ का विलय किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। प्रभावित छात्रों को लीड स्कूल में प्रवेश पर एकमुश्त सुविधा भत्ता भी प्रदान करने की बात कही गई है।
मध्य प्रदेश: पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं। सरकार नामांकन में गिरावट को लेकर चिंतित है और कलेक्टरों को अनमैप किए गए विद्यार्थियों को फिर से स्कूलों में नामांकित करने के निर्देश दिए हैं।
हरियाणा: हरियाणा भी उन राज्यों में से एक है जहां सरकारी स्कूलों को बंद करने की नीतिगत प्रक्रिया लागू की गई है।
राष्ट्रीय स्तर पर डेटा: संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में देश भर में 89,441 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, जिनमें से 61% यूपी और एमपी में हैं।
चिंताएं और नकारात्मक प्रभाव:
जैसा कि आपने अपनी पिछली प्रतिक्रिया में भी कहा था, यह प्रक्रिया कई गंभीर चिंताएं पैदा करती है:
शिक्षा तक पहुंच का संकट: खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, छोटे बच्चों को अब स्कूल तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है, जिससे ड्रॉपआउट दर बढ़ सकती है। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6-14 वर्ष के बच्चों को 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध कराने के प्रावधान का उल्लंघन माना जा रहा है।
वंचित और गरीब बच्चों पर असर: जिन परिवारों के पास परिवहन के साधन नहीं हैं या जो अपने बच्चों को दूर नहीं भेज सकते, उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो सकते हैं।शिक्षकों की नौकरी और स्थानांतरण: स्कूलों के विलय से शिक्षकों के स्थानांतरण या यहां तक कि सरप्लस होने की समस्या भी सामने आती है।
सामुदायिक स्वामित्व का नुकसान: छोटे स्थानीय स्कूल अक्सर अपने समुदाय से गहराई से जुड़े होते हैं। उनके बंद होने से सामुदायिक भागीदारी कम हो सकती है।
गुणवत्ता सुधार की गारंटी नहीं: केवल स्कूलों को मिलाने से स्वचालित रूप से गुणवत्ता में सुधार नहीं होता। इसके लिए प्रभावी शिक्षण, पर्याप्त शिक्षक, अच्छा पाठ्यक्रम और सीखने के अनुकूल माहौल जैसी मूलभूत चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है।
संक्षेप में, स्कूलों को बंद करने और विलय करने की यह प्रक्रिया भारत में शिक्षा के परिदृश्य को बदल रही है। जबकि सरकार इसे संसाधनों के कुशल उपयोग और गुणवत्ता सुधार के रूप में देखती है, वहीं आलोचक इसे शिक्षा तक पहुंच में कमी और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए शिक्षा के अवसरों को कम करने के रूप में देखते हैं। इस नीति का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा, यह देखने के लिए अभी समय लगेगा, लेकिन यह निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण और बहस का विषय बना हुआ है।
(लेखक पूर्व कुलपति कानपुर , गोरखपुर विश्वविद्यालय , विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर रह चुके हैं)
 Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal
Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal